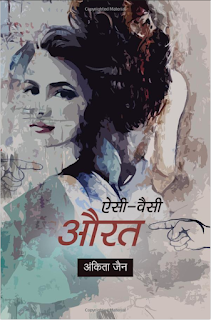|
| पुस्तक का आवरण पृष्ठ |
मैंने सम्भवतः दो वर्ष पहले इकिगाई नामक पुस्तक का नाम सुना था और भविष्य में इसे कभी पढ़ने का निर्णय लिया था। इसी वर्ष फ़रवरी माह के पहले दिन ही मैंने यह पुस्तक क्रय कर ली और सोचा था कि कभी रेलयात्रा के दौरान पढ़ूँगा। जून माह के प्रथम सप्ताह में मैंने इसे पढ़ने का निर्णय लिया और आज इसे पूर्णतः पढ़ लिया। यह हल्के नीले रंग के आवरण वाली पुस्तक है जिसपर अंग्रेज़ी में सबसे उपर बड़े काले अक्षरों में THE INTERNATIONAL BESTSELLER (अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर) लिखा है। उसके ठीक नीचे काले और श्वेत रंग में एक चित्र बना हुआ है जो किसी वृक्ष की टहनी जैसा प्रतीत हो रहा है। इसके नीचे पुस्तक का शीर्षक IKIGAI और फिर जापानी भाषा में 生き甲斐 लिखा हुआ है। ठीक इसके बाद The Japanese Secret to a Long and Happy Life (लम्बे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य) एवं एकदम नीचे HÉCTOR GARCÍA AND FRANCESC MIRALLES (हेक्टर गार्सिया और फ़्रान्सेस्क मिरालेस) लिखा हुआ है। मुझे आवरण पृष्ठ पर यह सुन्दर लगा कि सबसे उपर और सबसे नीचे वाली पंक्ति के अतिरिक्त सबकुछ उपर उभरा हुआ है। पुस्तक के पिछले आवरण पृष्ठ पर भी अंग्रेज़ी में बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसमें बार-कोड उभरे हुये हैं तथा एक चित्र (वैन-ग्राफ़) उभरा हुआ है। बार-कोड के निकट पुस्तक का मुल्य £12.99 लिखा हुआ है। यह चित्र चार वृत्तों से मिलकर बना हुआ है जिनके मध्य में अंग्रेज़ी में इकिगाई लिखा हुआ है और चारों वृत्तों में क्रमशः What you love (आपका प्यार), What you are good at (आप जिसमें अच्छे हैं), What you can paid for (आप जिसके लिए भुगतान कर सकते हैं) और What the world needs (दुनिया को क्या चाहिए) लिखा हुआ है। इसके मध्य में प्रत्येक दो वृत्तों के अंतर्वेशी स्थानों पर भी कुछ शब्द लिखे हुये हैं जो पहले दो के मध्य PASSION (भावावेश), दूसरे और तीसरे के मध्य PROFESSION (वृत्ति), तीसरे और चौथे के मध्य VOCATION (व्यवसाय) तथा चौथे और पांचवे के मध्य MISSION (ध्येय) लिखा हुआ है। यह वैन-ग्राफ़ पुस्तक के अन्दर भी पृष्ठ संख्या 9 पर भी है। पुस्तक के अन्दर के पृष्ठों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है लेकिन सस्ते में ऐसा पृष्ठ मिलना भी अच्छा है। पुस्तक के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ़्रान्सेस्क मिरालेस हैं और मेरे पास उपलब्ध अंग्रेज़ी अनुवाद हीदर क्लेरी (Heather Cleary) ने किया है। पुस्तक का प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस यूके है।
पुस्तक के शुरूआती पृष्ठों में पुस्तक की कॉपीराइट की जानकारी, लेखक, अनुवादक, प्रकाशक आदि की जानकारी है और इसके बाद एक जापानी कहावत लिखी हुई है, "Only staying active will make you want to live a hundred years." अर्थात् केवल सक्रिय बने रहने से ही आप सौ साल तक जीने की इच्छा रख सकेंगे। इसके पश्चात् पुस्तक में अनुक्रमणिका दी हुई है। पुस्तक का मूल भाग प्रस्तावना से आरम्भ होता है। कुछ पृष्ठ के बाद पुस्तक में वो नौ भाग/पाठ हैं जिनमें मूल सामग्री है और अंत में उपसंहार भी दिया गया है। पाँच पृष्ठ के उपसंहार के पश्चात् टिप्पणियों के नाम पर पुस्तक लिखने में काम लिए गये स्रोतों का विवरण है। इन स्रोतों में कुछ वेबसाइट और कुछ पुस्तकें भी शामिल हैं। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकों का सुझाव दिया गया है जिनसे लेखक प्रभावित हैं। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ में लेखकों के बारे में लिखा है। इसके अनुसार हेक्टर गार्सिया का जन्म स्पेन में हुआ और वो जापान के नागरीक हैं और दशकों से निवास कर रहे हैं। उन्होंने जापानी संस्कृति से सम्बंधित विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं। दूसरे लेखक फ़्रान्सेस्क मिरालेस भी विभिन्न पुस्तकों के लेखक रहे हैं। उन्होंने यह पुस्तक लिखने से पहले जापान के सैकड़ों लोगों के साक्षात्कार किये। यदि आप पुस्तक पढ़ने में रूचि रखते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ने का सुझाव देना चाहता हूँ।
पुस्तक की प्रस्तावना में इकिगाई को परिभाषित किया गया है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ उपर वर्णित वैन-ग्राफ़ के अनुसार है। इसे हिन्दी में "जीवन का कारण" के रूप में कह सकते हैं। वैन-ग्राफ़ के सबसे बीच के भाग को इकिगाई के रूप में वर्णित किया गया है। रहस्यमयी दुनिया में हम अपने आनन्द के कारणों को भूल जाते हैं और जल्दी ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेखकों के अनुसार सेवानिवृत्ति का अर्थ कार्य निवृत्ति नहीं होना चाहिए। कार्य से निवृत्ति का अर्थ अपने आप को मृत घोषित करने जैसा है।
पुस्तक के सबसे पहले पाठ में बढ़ती आयु के साथ जवान रहने का तरिका समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें स्वयं की रूचि को पहचाने के बारे में बताया है। अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहिए। आपके लिए कौनसा काम सबसे अच्छा है वो आपको खोजना चाहिए। इसके बाद आपको वो कार्य खोजना चाहिए जो आपको आकर्षित करता है। आप कौनसा काम करने में बेहतर हैं, प्राकृतिक रूप से आप कौनसा कार्य करने में बहुत अच्छे हैं? क्या आपको किसी कार्य के लिए धन मिलता है? उदाहरण के लिए आपको भोजन तैयार करना पसन्द हो सकता है लेकिन इसके लिए क्या आपके घर पर पैसा मिलता है? आवश्यक नहीं कि आपको अपने इस कार्य के लिए धन मिले अतः कोई ऐसा काम खोजें जिसके लिए आपको धन प्राप्ति हो सके। आपको ऐसा काम खोजना चाहिए जो अन्य लोगों के लिए उपयुक्त हो। आपके कभी कार्य-मुक्त नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी आयु वाले द्वीप के बारे में बताया गया है। इसके बाद पुस्तक में वो पाँच स्थान लिखे हैं जहाँ लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं और अच्छा भोजन करते हैं। इसके साथ ही उनकी आयु बहुत लम्बी होती है। पुस्तक में 80 प्रतिशत नियम के बारे में बताया है जिसके अनुसार पेट को भोजन से पूर्णतः भरने से मना किया गया है। इसके अनुसार आपको जितनी भूख हो, उससे थोड़ा कम भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोवाई लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिनका जीवन से जुड़ाव बताया है।
दूसरे पाठ में उन छोटे-छोटे कार्यों के बारे में बताया है जो जीवन को खुशियाँ देते हैं। इसमें जीवन में अतिरिक्त वर्ष जोड़ने के बारे में लिखा हुआ है। एक खरगोस का उदाहरण देते हुये इसमें उदाहरण दिया गया है कि एक खरगोस एक निश्चित सीमा पार करते ही मर जायेगा, लेकिन उसके एक मीटर चलने पर वो सीमा कुछ सेंटीमीटर आगे खिसक जाती है, उस स्थिति में खरगोस की आयु में वृद्धि हो जायेगी। यदि यह सीमा रेखा भी उसी गति से आगे बढ़ने लग जाये जिस गति से खरगोस आगे बढ़ रहा है तो वो खरगोस अमर हो जायेगा। इस सीमा रेखा को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को सक्रिय रखना होगा और शरीर को युवा रखें। तनाव लेने से जीवन कम हो जाता है अतः तनाव से दूर रहने के बारे में भी लिखा गया है। तनाव कैसे काम करता है यह भी इसमें समझाया है और इसके लिए गुफाओं में रहने वाले मानव और वर्तमान मानव के मध्य तुलना भी दी गयी है। तनावमुक्त रहने के लिए कैसे दिमाग को तैयार करें? इस पाठ के अनुसार तनाव का अल्प मात्रा में होना भी आवश्यक है अन्यथा हम बहुत आलसी हो जायेंगे। एक ही जगह लम्बे समय तक बैठे रहने से भी आयु जल्दी बढ़ती है अर्थात् हम बुड्ढ़े हो जाते हैं। इस पाठ के अनुसार आपकी त्वचा आपकी आयु को दिखाती है। त्वचा को जवान रखने के लिए आपको 9 से 10 घंटे तक सोना चाहिए और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना चाहिए। आयु को बढ़ने से रोकने का क्या तरिका है और लम्बे जीवन के लिए कविता भी लिखी है।
पुस्तक के तीसरे पाठ में लोगोथेरेपी के बारे में लिखा है। इसमें जीवन में उद्देश्य खोजने के बारे में लिखा है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक के बारे में लिखा है जो अपने मरीज को सबसे पहले पूछता है कि आप आत्महत्या क्यों नहीं करना चाहते और यहाँ रोगी कुछ अच्छे कारण खोज लेता है। लेकिन लोगोथेरेपी में व्यक्ति को इस तरह के प्रश्नों की आवश्यकता नहीं होती और वो सरलता से अपने कारण खोज लेते हैं। इस तरह आपको अपने जीवन में कारण खोजने चाहिए जो आपके लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और लोगोथेरेपी में अंतर स्पष्ट किया गया है। इस पाठ में अपने लिए लड़ने के बारे में बताया गया है जिससे आप अपना महत्त्व समझ सको। इसके लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दू भी दिये गये हैं। इसके बाद इसमें कुछ विशिष्ट प्रकरण अध्ययन दिये गये हैं। इसी पाठ में आगे मोरिता थेरेपी के बारे में बताया है। यह बौद्ध धर्म के एक अनुयायी शोमा मोरिता द्वारा खोजी गयी चिकित्स के बारे में बताया गया है। इसमें मोरिता थेरेपी के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में बताया है जिसके अनुसार सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं और जीवन में कोई उद्देश्य खोजना चाहिए। मोरिता थेरेपी के चार चरण भी दिये हैं जिनके अनुसार पहला चरण पांच से सात दिन तक एकदम सभी से अलग और आराम से रहने के बारे में बताया है। सबसे अलग का अर्थ टेलीविजन, पुस्तक, दोस्त, परिवार और उन सभी उपकरणों से दूर रहने के लिए कहा गया है जिनका ध्वनि या बोलने से सम्बंध हो। अगले चरण में एक सप्ताह के लिए शांति से कुछ पुनरावृत्ति वाले कार्य करने के लिए लिखा गया है। तीसरे चरण में एक सप्ताह के लिए शारीरिक गतिविधि वाले कार्य करने के लिए लिखा गया है। इसके बाद चौथे चरण में वापस सामान्य जीवन जीने के बारे में कहा गया है। इसके बाद इसी पाठ में नैकान ध्यान के बारे में लिखा गया है और अंत में इससे इकिगाई से जोड़कर बताया गया है।
पुस्तक के चौथे पाठ में सभी कार्यों की निरंतरता के बारे में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि आप अपने कार्य के समय और मुक्त समय को अपनी संवृद्धि में कैसे शामिल कर सकते हैं। इस पाठ के शुरूआत में बताया गया है कि जब आप स्कीयन (skiing) का उदाहरण दिया है। मैं इस उदाहरण को एक कार चालक या सायकिल चलाने वाले से जोड़कर कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी स्कीयन नहीं किया। जब कार चलाते हैं तब हमारा ध्यान उसी समय और सामने होता है। कार चलाने से जो धूल उड़ रही है उसपर ध्यान नहीं देते और यदि उसे देखने लग गये तो दुर्घटना की सम्भावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जीवन में आपको इसी समय को देखना चाहिए। अपने जीवन में प्रवाह होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं के बारे में जानना चाहिए, यह भी जानना चाहिए कि जो करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कितना अच्छे से कर सकते हैं आदि। आपको कठिन कार्य चुनने चाहिए लेकिन इतने कठिन भी नहीं कि वो असम्भव हों। किसी काम को करने से पहले हमें इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें एक साथ बहुत काम नहीं करने चाहिए। एक साथ कई काम करने से समय बर्बाद होता है और हम किसी एक काम को भी ढ़ंग से नहीं कर पाते। जापान में निरंतरता के बारे में लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि जापान के लोग कैसे अपना उद्देश्य खोजकर उसके साथ चलते हैं। इसमें ताकुमी कला के बारे में बताया गया है कि कैसे कुछ स्क्रू (कील) जापान के कुछ लोग अपने हाथ से बनाते हैं और इसमें उनकी निपुणता बहुत अधिक है। अमेरिकी व्यापारी स्टीव जॉब्स के जापान यात्रा के बारे में लिखा गया है। इस पाठ में आलसी सरलता और कार्य की पूर्ण जानकारी के साथ सरलता के बारे में लिखा गया है। इसी पाठ में जिबली (Ghibli) की शुद्धता के बारे में भी लिखा गया है। इसके आगे इसमें विरक्ति के बारे में लिखा गया है कि विश्व में ऐसे विभिन्न लोग रहे हैं जिन्होंने मरते दम तक अपने इकिगाई को खोजकर उसके अनुसार ही कार्य किया। सांसारिक कार्यों का आनन्द लेने का तरिका भी यहाँ लिखा गया है। ध्यान के माध्यम से लघु अवकाश कैसे लें यह भी इसमें लिखा गया है। मानव कर्मकांडी होता है अतः हमें धार्मिक अथवा संस्कारी कार्यों में भी भाग लेना चाहिए जिससे हम लोगों से जुड़ेंगे और खुशियाँ बढ़ेंगी। इकिगाई के माध्यम से जीवन में निरंतरता प्राप्त करने के बार में भी लिखा है।
पाँचवे अध्याय में दीर्घायु लोगों के बारे में लिखा है। इसमें लम्बे जीवन जीने वाले कुछ लोगों के जीवन को लिखा गया है। मिसावो ओकावा (117 वर्ष) के बारे में लिखा है कि उनके अनुसार अच्छा भोजन और लम्बी नींद दीर्घायु होने का राज है। मारिया कैपोविला (116 वर्ष) के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया। ज्यां कैल्में (Jeanne Calment) (122 वर्ष) ने 120वें जन्मदिन पर कहा था कि वो अच्छे से सुन नहीं सकती, अच्छे से देख नहीं सकती, बुरा महसूस करती हैं लेकिन सबकुछ अच्छा है। वाल्टर ब्रूनिंग (114 वर्ष) के अनुसार आप अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त रखोगे तो आप दीर्घायु होने में सफलता प्राप्त करोगे। अलेक्जेंडर इमिच (111 वर्ष) के अनुसार उन्हें उनके दीर्घायु होने का कारण ज्ञात नहीं था। माउंट फुजी ने अपने सौंवे जन्मदिन पर बतया कि उन्होंने 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कुछ खास नहीं किया लेकिन इसके बाद प्रकृति को समझा और उसके अनुसार ढ़लते चले गये।
छठे अध्याय में जापन में जीवन का शतक लगा चुके लोगों के बारे में है जिसमें जापान के लोगों की खुशियों और दीर्घायु होने का कारण वहाँ की परम्पराओं और कहावतों को कहा है। इसमें जापान के ओगिमी नामक एक गाँव का उल्लेख है। लेखक ने इस दूरस्त गाँव में पहुँचने के अपने अनुभव साझा किये हैं। वहाँ गाँव के सामाजिक जीवन का उल्लेख किया गया है जो भोजन से भी जुड़ा हुआ है। लेखक ने एक जन्मदिन का उत्सव मनाने का उल्लेख किया जिसमें सबसे युवा व्यक्ति 83 वर्ष का था। उस गाँव में सभी लोग प्रत्येक दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। यह गाँव ओकिनावा नामक प्रांत में स्थित है अतः लेखक ने आगे इस प्रान्त में प्रचलित धर्मों के बारे में बताया और जिससे वहाँ के लोगों के रहन-सहन का धर्म से सम्बंध समझा जा सके। यहाँ लोग अपना जीवन शांति से व्यतीत करते हैं। लेखक ने यहाँ नौ सौ लोगों का साक्षात्कार किया जिसमें उन्होंने प्रेक्षित किया कि वहाँ के लोगों के अनुसार हृदय को जवान रखने के लिए आवश्यक है कि आप मुस्कराते हुये लोगों से मिलो। अच्छी आदतों को अपने जीवन में जोड़ो। हमेशा अपने दोस्तों का साथ निभावो। जीवन को दौड़ की तरह समझने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आशावादी रहो।
सातवें अध्याय में इकिगाई आहार के बारे में लिखा गया कि दीर्घायु लोग क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। इस पाठ के पहले ही पृष्ठ में सन् 1960 से 2000 तक जापानी प्रान्त ओकिनावा, जापान, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्यासा के बढ़ने का आरेख को दिखाया है इसके अनुसार ओकिनावा हमेशा ही अन्य स्थानों से आगे रहा है। इसमें ओकिनावा चमत्कारी आहर के बारे में लिखा गया है। इसी अध्याय में हारा हाची बु के नाम पर 80 प्रतिशत वाला नियम पुनः दोहराया गया है। इसमें बताया गया है कि लोग भोजन के बाद मिठा खाते हैं लेकिन लम्बे जीवन के लिए इस आदत को बदलना चाहिए और मिठाई को बंद कर देना चाहिए। यदि बंद नहीं कर सकते तो कम करना चाहिए। इसके अगले भाग में उपवास के महत्त्व को समझाया गया है। ओकिनावा के आहार में 15 प्रति-उपचायकों के बारे में लिखा गया है। इसके पश्चात् सैंपिन चाय के बारे में लिखा है जो 15 प्रति-उपचायकों में से एक है। सैंपिन चाय हरी चाय और चमेली के फुलों के मिश्रण से बनती है। इसके लाभ यहाँ लिखे गये हैं। इसके बाद शिकुवासा नामक एक खट्टे फल का विवरण है।
आठवें अध्याय में सौम्य अथवा कोमल गतिविधियों के बारे में बताया गया है जो पूर्व (पूर्वी देशों) से हमें मिली हैं। इस अध्याय के अनुसार दीर्घायु लोग वो नहीं हैं जो बहुत अधिक कसरत/अभ्यास करते हैं बल्कि वो हैं जो लगातार कोई न कोई गतिविधि करते रहते हैं। इस पाठ में योग रेडियो ताइसो, योग, थाई ची, चीगोंग (Qigong) और शियात्सु के बारे में लिखा गया है। इन सभी को पहले बताया गया है कि यह गतिविधि मूल रूप से कहाँ की है? इसको करने के कितने माध्यम हैं? इसके बाद प्रत्येक के साथ किसी एक विधि को अच्छे से चित्रित रूप में समझाया गया है। इन चित्रों को देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये कठिन कार्य नहीं है बल्कि किसी भी आयुवर्ग का कोई भी व्यक्ति इन्हें दोहरा सकता है। ये साँस लेने का तरिका है जो जीवन को दीर्घायु बनाता है।
नौंवे अध्याय लचीलापन और वबी-सबी में तनाव और चिंता रहित जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बारे में लिखा गया है। इसमें पहले जीवन में लचीलापन रखने के बारे में लिखा गया है। यहाँ बौद्ध और स्टोइक दर्शन के बारे में लिखा गया है। पहले बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है जिसके अनुसार कपिलवस्तु में धनाढ़य परिवार में जन्मे और पालन-पोषण के बाद गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया और अपने आप को कठिन स्थित में डाला लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि यह मार्ग उनके लिए नहीं है अतः उन्होंने बाद में मध्यम मार्ग निकाला। इसी तरह उन्होंने स्टोइक दर्शन के बारे में बताया है और उनके मूल से उन्हें समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे लेख में उस स्थिति का वर्णन किया है कि जीवन में सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और उसका सामना कैसे करें। स्टोइक दर्शन के अनुसार स्वस्थ भावनाओं के लिए ध्यान देने को समझाया है। बौद्ध एवं स्टोइक दर्शन दोनों में ही वर्तमान में रहने पर ध्यान दिया गया है न कि भूतकाल या भविष्य को लेकर परेशान होना। इसके बाद जापानी अवधारणा वाबी-साबी और इचिगो इचीई के बारे में बताया है जिसके अनुसार केवल यह समय ही सर्वश्रेष्ठ है और हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए। इसके बाद लचीलापन से आगे एंटीफ्रैगिलिटी अर्थात् प्रति-भंगुरता के बारे में लिखा गया है। यहाँ हाइड्रा की अवधारणा के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार उसका एक सिर काटने पर वो दोगुणा ताकत के साथ दो रूप में अवतरित हो जाता है। इसी तरह अपने जीवन में नकारात्मक अवधारणायें बढ़ती हैं और इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में बताया गया है। इस कार्य को तीन चरणों में पूरा करने का तरिका बताया है।
 |
| आवरण पृष्ठ का पिछला भाग |
उपसंहार में बताया है कि सभी का इकिगाई अलग-अलग होता है और हमें अपना इकिगाई स्वयं को पहचानना होता है। इसके लिए ओगिमी के इकिगाई के दस नियम लिखे गये हैं जो निम्नलिखित हैं:
- सक्रिय रहो, कार्य मुक्त न हों
- धीमे रहो, जल्दबाजी से मुक्त रहो
- पेट को पूरी तरह मत भरो
- अच्छे दोस्तों के साथ रहो
- अपने अगले जन्मदिन के लिए तैयार रहो
- मुस्कराहट साथ में रखो
- प्रकृति से जुड़े रहो
- अपनी प्रत्येक साँस के लिए अपने पूर्वजों और प्रकृति को धन्यवाद दो
- वर्तमान समय का आनन्द लो और
- अपने इकिगाई का अनुशरण करो।
कुल मिलाकर मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी।